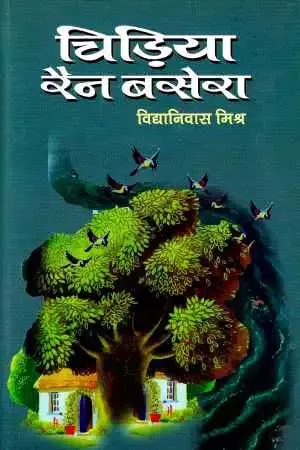|
यात्रा वृत्तांत >> चिड़िया रैन बसेरा चिड़िया रैन बसेराविद्यानिवास मिश्र
|
406 पाठक हैं |
||||||
‘चिड़िया रैन बसेरा’ जिन-जिन स्थानों में नीड़ बनाता रहा या नीड़ मिलते गए उन स्थानों और उनसे जुड़े लोगों का पार्श्व चित्र है...
Chidiya Rain Basera
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भूमिका
‘चिड़िया रैन बसेरा’ जिन-जिन स्थानों में नीड़ बनाता रहा या नीड़ मिलते गए उन स्थानों और उनसे जुड़े लोगों का पार्श्व चित्र है। इसका आधार न कोई डायरी है, न कोई नोट बुक। इसका आधार प्रत्यक्ष की तरफ अनुभूत होने वाली स्मृति है। ऐसे प्रत्यक्ष में यह नहीं लगता कि ये स्थान, ये लोग व्यतीत हो गये हैं; ऐसा लगता है कि अभी भी सामने हों और संवाद के लिए उदग्र हों। वैसे इसकी योजना बहुत दिनों से मन में थी। इस शीर्षक से एक निबंध भी लिखा था; पर इसकी कड़ियों को आगे बड़ाने का श्रेय ‘जनसत्ता’ के संपादक ओम थानवी को जाता है।
मैंने अपने जीवन के तिथि-क्रम से ये कड़ियाँ नहीं लिखीं। जो भी स्थान मेरे सामने किसी व्याज से आ गया तो उससे जुड़े हुए संस्मरण अनायास चित्रपट की रील की तरह उभरने लगे। इन कड़ियों में क्रम का कोई महत्त्व नहीं है। कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है जैसा फ्लैशबैक में होता है। एक तरह से सोचें तो ये सभी कड़ियाँ फ्लैश-बैक हैं। केवल अतर्कित मन की रागात्मिका वृत्ति कभी किसी शहर से जुड़कर कुछ कहना चाहती है, कभी किसी गाँव से। कभी किसी शहर से।
सभी स्थानों के बारे में अभी तक नहीं लिख पाया हूँ। कभी लिख पाऊँगा, यह आश्वासन भी नहीं दे सकता। हाँ, उन्हें भी लिखने की इच्छा है। वे स्थान वैसे हैं जहाँ पर पंद्रह दिन, एक महीना रहना हुआ है या वहाँ स्नेह-सूत्रों के कारण बार-बार जाना हुआ है। ये स्थान देश में भी हैं, विदेश में भी हैं।
अंतिम कड़ी के रूप में मैं काशी के बारे में लिखना चाहता हूँ, जहाँ बीच-बीच में कई बार अंतराल आए हैं। और वहीं लौटना लगभग तैंतीस वर्षों से अपरिहार्यत: होता रहा है। इसीलिए काशी एक प्रकार से मेरे लिए अतीत से अधिक भविष्यत् है, वर्तमान तो है ही। सोचता हूँ, केवल काशी पर और काशी निवास में आए अंतरालों पर अलग से लिखूँ, जब भी लिखूँ।
इस संग्रह की कड़ियाँ जंजीर के रूप में एक-दूसरे में जकड़ी हुई नहीं है। ये कड़ियाँ तुलसीदासजी से उपमा उधार लूँ-आकाशगंगा के नक्षत्रों की तरह ओर-छोर तक पसरी हुई हैं। इनमें से प्रत्येक की दूसरे से दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में नापी जा सकती हैं; पर धरती से जब इन्हें देखते हैं तो ये सब नदी की अविच्छिन्न धार दिखती हैं। भरत के प्रसंग में यह उपमा अयोध्याकांड में आयी है। वहाँ तो एक राम के साथ जुड़ी हजारों स्मृतियाँ आकाशगंगा बन गई हैं; पर मेरे आकाश में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जगहें हैं, उन जगहों के इतने परिदृश्य हैं, उन लोगों के अलग-अलग व्यक्तित्व के कोर-कगार हैं, पर जाने किस जादू के बल से झरनेवाली पतली-सी, पर तेज प्रवाह वाली धार बन गए हैं। उनके साथ चलने का अर्थ होता है उन्हीं का हो जाना।–अर्थात् उनके साथ चलने की बात आते ही स्वयं अपनी निजता खो देना, विशेष रूप से निजता का अकेलापन तो विसर्जित ही कर देना।
मैंने विराम अपने जनपद के मुख्य शहर गोरखपुर में लिया है, सिर्फ इसलिए कि परिवार में सबसे बड़ा होने के कारण और गोरखपुर में ही परिवार के सभी उत्सव संचालित होने के कारण गोरखपुर एक प्रकार की गार्हस्थिक नियति है। यह बिलकुल तय है कि जगहों से जुड़े बहुत से नाम छूटे होंगे, उन नामों का महत्त्व कुछ कम नहीं है; पर जिन्हें छोड़ना चाहें और न छूट पाएँ, ऐसे नाम नहीं छूटे हैं। वे मेहँदी के रंग की तरह बार-बार धुलने पर वैसे ही नगीने की तरह विजड़ित हैं। मैंने जानबूझकर अप्रिय प्रसंगों और उनसे जुड़े लोगों की चर्चा नहीं की है, क्योंकि जीवन की इस ढलती वेला में सिमटते हुए प्रकाश को ही अपने में भरना शोभा देता है, उस सिमटते हुए प्रकाश के साथ सिमटती हुई चिड़ियों की आवाजों को भरना अधिक सहज होता है। दंश को लेकर कुंठित होना और मन में कलुष पालना बहुत व्यर्थ लगता है, इसलिए ये कड़ियाँ न तो आत्मकथा हैं, न संस्मरण, ये बस स्मृति और प्रत्यक्ष की आँखमिचौनी के खेल की न थमनेवाली दौड़ हैं। अधिकांशत: यह पुस्तक बोलकर लिखाई गई है। गणेश का काम कइयों ने किया है-प्रमुख रूप से उदीयमान कवि-कथाकार प्रकाश उदय ने। अंतिम कड़ी आगरा में राजेंद्र पुष्प ने लिखी है। भूमिका के लिए अंतिम गणेश अनंतकीर्ति तिवारी बने। मैं स्वयं नहीं जानता, कैसे साल भर में यह किताब पूरी हुई। जीवन इतनी धाराओं में बँटा हुआ है कि कोई पुस्तक पूरी हो जाती है तो मैं इसे आश्चर्य ही मानता हूँ। बस इसके आगे तो पाठक जानें।
मैंने अपने जीवन के तिथि-क्रम से ये कड़ियाँ नहीं लिखीं। जो भी स्थान मेरे सामने किसी व्याज से आ गया तो उससे जुड़े हुए संस्मरण अनायास चित्रपट की रील की तरह उभरने लगे। इन कड़ियों में क्रम का कोई महत्त्व नहीं है। कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है जैसा फ्लैशबैक में होता है। एक तरह से सोचें तो ये सभी कड़ियाँ फ्लैश-बैक हैं। केवल अतर्कित मन की रागात्मिका वृत्ति कभी किसी शहर से जुड़कर कुछ कहना चाहती है, कभी किसी गाँव से। कभी किसी शहर से।
सभी स्थानों के बारे में अभी तक नहीं लिख पाया हूँ। कभी लिख पाऊँगा, यह आश्वासन भी नहीं दे सकता। हाँ, उन्हें भी लिखने की इच्छा है। वे स्थान वैसे हैं जहाँ पर पंद्रह दिन, एक महीना रहना हुआ है या वहाँ स्नेह-सूत्रों के कारण बार-बार जाना हुआ है। ये स्थान देश में भी हैं, विदेश में भी हैं।
अंतिम कड़ी के रूप में मैं काशी के बारे में लिखना चाहता हूँ, जहाँ बीच-बीच में कई बार अंतराल आए हैं। और वहीं लौटना लगभग तैंतीस वर्षों से अपरिहार्यत: होता रहा है। इसीलिए काशी एक प्रकार से मेरे लिए अतीत से अधिक भविष्यत् है, वर्तमान तो है ही। सोचता हूँ, केवल काशी पर और काशी निवास में आए अंतरालों पर अलग से लिखूँ, जब भी लिखूँ।
इस संग्रह की कड़ियाँ जंजीर के रूप में एक-दूसरे में जकड़ी हुई नहीं है। ये कड़ियाँ तुलसीदासजी से उपमा उधार लूँ-आकाशगंगा के नक्षत्रों की तरह ओर-छोर तक पसरी हुई हैं। इनमें से प्रत्येक की दूसरे से दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में नापी जा सकती हैं; पर धरती से जब इन्हें देखते हैं तो ये सब नदी की अविच्छिन्न धार दिखती हैं। भरत के प्रसंग में यह उपमा अयोध्याकांड में आयी है। वहाँ तो एक राम के साथ जुड़ी हजारों स्मृतियाँ आकाशगंगा बन गई हैं; पर मेरे आकाश में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जगहें हैं, उन जगहों के इतने परिदृश्य हैं, उन लोगों के अलग-अलग व्यक्तित्व के कोर-कगार हैं, पर जाने किस जादू के बल से झरनेवाली पतली-सी, पर तेज प्रवाह वाली धार बन गए हैं। उनके साथ चलने का अर्थ होता है उन्हीं का हो जाना।–अर्थात् उनके साथ चलने की बात आते ही स्वयं अपनी निजता खो देना, विशेष रूप से निजता का अकेलापन तो विसर्जित ही कर देना।
मैंने विराम अपने जनपद के मुख्य शहर गोरखपुर में लिया है, सिर्फ इसलिए कि परिवार में सबसे बड़ा होने के कारण और गोरखपुर में ही परिवार के सभी उत्सव संचालित होने के कारण गोरखपुर एक प्रकार की गार्हस्थिक नियति है। यह बिलकुल तय है कि जगहों से जुड़े बहुत से नाम छूटे होंगे, उन नामों का महत्त्व कुछ कम नहीं है; पर जिन्हें छोड़ना चाहें और न छूट पाएँ, ऐसे नाम नहीं छूटे हैं। वे मेहँदी के रंग की तरह बार-बार धुलने पर वैसे ही नगीने की तरह विजड़ित हैं। मैंने जानबूझकर अप्रिय प्रसंगों और उनसे जुड़े लोगों की चर्चा नहीं की है, क्योंकि जीवन की इस ढलती वेला में सिमटते हुए प्रकाश को ही अपने में भरना शोभा देता है, उस सिमटते हुए प्रकाश के साथ सिमटती हुई चिड़ियों की आवाजों को भरना अधिक सहज होता है। दंश को लेकर कुंठित होना और मन में कलुष पालना बहुत व्यर्थ लगता है, इसलिए ये कड़ियाँ न तो आत्मकथा हैं, न संस्मरण, ये बस स्मृति और प्रत्यक्ष की आँखमिचौनी के खेल की न थमनेवाली दौड़ हैं। अधिकांशत: यह पुस्तक बोलकर लिखाई गई है। गणेश का काम कइयों ने किया है-प्रमुख रूप से उदीयमान कवि-कथाकार प्रकाश उदय ने। अंतिम कड़ी आगरा में राजेंद्र पुष्प ने लिखी है। भूमिका के लिए अंतिम गणेश अनंतकीर्ति तिवारी बने। मैं स्वयं नहीं जानता, कैसे साल भर में यह किताब पूरी हुई। जीवन इतनी धाराओं में बँटा हुआ है कि कोई पुस्तक पूरी हो जाती है तो मैं इसे आश्चर्य ही मानता हूँ। बस इसके आगे तो पाठक जानें।
विद्यानिवास मिश्र
चिड़िया रैन बसेरा
बसेरे की सुधि दो ही समय आती है-या तो तब जब आदमी थककर चूर होता है या फिर तब जब बसेरा सदा के लिए छूटने को होता है। आज जिस मोड़ पर मैं हूँ उसमें एक ओर तो बसेरा का बड़ा मोह होता है, या यों कहें, बसेरों का बड़ा मोह होता है, क्योंकि बसेरे भी बहुत बने, उजड़ा कोई नहीं; पर मेरा कुछ-न-कुछ अंश जरूर उजड़ता गया है। कबीर का पद याद आता है, जिसका अर्थ यही है-‘हंस’ सरोवर कैसे छोड़े, जिस सरोवर में मोती चुगता रहा, जिसमें रहकर कमलों से केलि की, वह सरोवर भी छूट रहा है और वह कैसे छूटे ?
ऊँचे गगन का निमंत्रण है तो भी क्या ? खुलेपन का निमंत्रण है तो क्या ? अमरत्व का निमंत्रण है तो भी क्या ? मोक्ष का निमंत्रण है तो भी क्या ? सरोवर मानसरोवर भी नहीं था। मामूली पोखर, जिसमें जल का अंश नाम मात्र को रह जाता है, धूप है-झलमल चमकने भर को। जल कम, कीच ही अधिक रहती थी। कमल जरूर खिलते थे और परिश्रम से खिलते थे। ऐसे पोखर को भी छोड़ते समय दर्द तो होता ही है।
ऊँचे गगन का निमंत्रण है तो भी क्या ? खुलेपन का निमंत्रण है तो क्या ? अमरत्व का निमंत्रण है तो भी क्या ? मोक्ष का निमंत्रण है तो भी क्या ? सरोवर मानसरोवर भी नहीं था। मामूली पोखर, जिसमें जल का अंश नाम मात्र को रह जाता है, धूप है-झलमल चमकने भर को। जल कम, कीच ही अधिक रहती थी। कमल जरूर खिलते थे और परिश्रम से खिलते थे। ऐसे पोखर को भी छोड़ते समय दर्द तो होता ही है।
हंसा प्यारे सरवर तजि कहँ जाय
जेहि सरवर बिच मोतिया चुगते, बहुविधि केलि कराय
सूखे ताल पुरइन जल छाड़े, कमल गए कुम्हिलाय
कहे कबीर जो अबकी बिछुरे, बहुरि मिलो कब आए।
जेहि सरवर बिच मोतिया चुगते, बहुविधि केलि कराय
सूखे ताल पुरइन जल छाड़े, कमल गए कुम्हिलाय
कहे कबीर जो अबकी बिछुरे, बहुरि मिलो कब आए।
बसेरा मेरा बनाया हुआ कोई नहीं था। बसेरा बनाने की कभी इच्छा जगी भी, कुछ नक्शा बना भी, पर जाने क्यों कंकड़-पत्थर जोड़ने का उत्साह नहीं हुआ। जोड़ते देखने में मजा जरूर आता था। बचपन में घर बनाने का खेल खेलने में भी मजा आता था। जेठ की दोपहरी में घर के पिछवाड़े ईंटों का अंबार लगा था। उन्हीं को जैसे-तैसे एक के ऊपर एक रखकर और माटी के गारे से चिपकाकर घर बना लेता था; अपनी छोटी बहनों का सहयोग लेता था। उनके लिए उनके मुताबिक उनके गुड्डे-गुड़ियों के लिए बसेरा बनाता था। किसी को न लू लगती थी, न थकान। घर की योजना पर बहस होती थी। बड़ी मुश्किल से तय होता था कि दरवाजा किधर होगा, खिड़कियां कैसी होगीं। घर दो-मंजिला होगा। सीढ़ी बनेगी। और तब घर बनना शुरू होता था। सारी दोपहर मेहनत करने पर भी घर कभी-ही-कभी बन पाता था और बन भी जाता था तो किसी-न-किसी की कौतिकी क्रीड़ा से ढह भी जाता था। ऐसे अत्यंत क्षणभंगुर घरों के निर्माण के अलावा किसी दूसरे घर के निर्माण का भाग्य मुझे मिला नहीं। हमेशा दूसरों के बने-बनवाए घरों में ही रहा। गाँव का घर छोड़ भी दें तो लंबे समय तक किराए के घरों में रहा। ईश्वरीय कृपा को बार-बार स्मरण करता रहा कि ‘यह बखरी रहियत है भारे की’, यह बखरी, यह घर, यह शरीर सब भाड़े के हैं। अगर भाड़े के इन सब घरों को जोड़ते चलें तो भय है कि कोई-न-कोई छूट जाएगा।
कम-से-कम मन से क्रम ठीक नहीं बन पाएगा। तब भी इन सभी घरों का, घरों की कोई-न-कोई गंध, कोई सुवास, कोई-न-कोई स्पर्श अभी तक प्राणों में हो, रोम-रोम में हो। इनमें से कोई भी ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं पराया कह सकूँ। कोई भी इनमें से मेरा नहीं है। पर मेरा जितना अपना होता है उससे अधिक अपना है। शायद इसीलिए इन सबके साथ बड़ा खट्टा-मीठा अनुभव जुड़ा हुआ है। भोजपुरी में इसे ‘अमलोन’ कहते हैं। और वैसा स्वाद अभी भी रसना में है, ललक बनी हुई है। अपभ्रंश में इसी को ‘अंबण’ कहते हैं और प्रिय के संदर्भ में किसी दोहे में यह कहा गया है कि प्रिय ने अमलोन स्वाद लगा दिया है। उसके लिए मोह अब भी है, मुँह में पानी भर आता है। कुछ ऐसा ही संबंध है कुछ ऐसी ही लाग...बसेरों में से प्रत्येक बसेरे ने लगा रखी है। मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता हूँ और दार्शनिक भाव से सोचना चाहता हूँ, ‘घर वही है जो थके को रैन भर का हो बसेरा।’ दार्शनिक भाव से वक्तव्य देना तो आसान है। ममता का आदमी के लिए खोखला होना कठिन है। ममता के त्याग की बात करते हैं। ममता का त्याग करेंगे तो आदमी कहाँ रहेगा। ममताओं का जाल जितना ही फैलता जाता है उतना ही आदमी का विस्तार होता है। ममता जितना बाँधती है उतना ही उसे कहीं मुक्त भी करती है। जितना अधिक जाल है, उस जाल को बढ़ाकर, तानकर तोड़ देने की कोशिश भी है, वह दायरा मात्र नहीं है। दायरों का ऐसा विस्तार है जिसमें दायरों की सीमा दिखती ही नहीं। जितनी वह कमजोरी है उससे अधिक आदमी की शक्ति है।
मैं यह सब विमर्श करते हुए दार्शनिक मुद्रा में फिर लौटना नहीं चाहता। मैं तो बस बसेरों की बात करना चाहता हूँ। बसेरों से अधिक, बसेरों को एक बार फिर, हर बार एक बसेरे में लौटकर, अपने को स्थापित करना चाहता हूँ। कर सकूँगा या नहीं, नहीं जानता। कोशिश करना चाहता हूँ। घर में रहनेवाला घर के बारे में नहीं सोचता। जितना घर से कई बार बाहर जाकर घर के बारे में सोचता है।
कोई पूछे, तुम्हारा घर कहाँ है ? तो मैं उत्तर देते समय लड़खड़ाने लगूँगा, किसे घर कहूँ ! जहाँ जन्म हुआ उसे, जो मेरे जन्म के दो-ढाई साल बाद ढहा दिया गया ? उसके बाद नया घर उठाया गया, उसे मानूँ ? छुट्टियों में ननिहाल के खंडहरनुमा घर में भारतेंदु काल के विपुल साहित्य के भंडार का आलोडन-विलोडन किया। अधिकतर समझ में नहीं आया। तरह-तरह के नाम आँखों के सामने तैरते हैं, उसे घर कहूँ, क्योंकि उस समय हिंदी में कुछ वैसा ही लिखने का मन जगा ? संस्कृत में जन्म हुआ। उसी ने मुझे पाला-पोसा और मैं उसी घर के कारण हिंदी के घर में चुपके से बैठने का संकल्प ले बैठा। या उसे घर कहूँ, जहाँ मैं रहा ? शहरवाले घर को घर कहूँ, जहाँ से मैंने स्कूली और प्रारंभिक शिक्षा पाई ? वहाँ चार घर बदले या घर इलाहाबाद के एक कोने से दूसरे कोने तक की अलग-अलग कोठरियों को घर कहूँ, जहाँ मैं ग्यारह वर्षों का समय कुछ अध्ययन और स्वावलंबनजीवी के संघर्ष में भिड़ा रहा ? या फिर विंध्य के दिन में तपते शाम, सियराते पहाड़ों-पत्थरों को फोड़कर बननेवाली नदियों, सिर से टकरानेवाली अटारियों और दरबारियों और भाषा के अतिशय विनम्रतावाली भाषा के बोलनेवाले, मित्रों के बीच पहले अजनबी की तरह सेवा छोड़ते-छोड़ते अपना पग दूसरे पड़ाव की ओर चला या फिर लखनऊ शहर के पं.भैया साहब श्रीनारायण चतुर्वेदी के उस मकान को जहाँ लखनऊ के सूचना विभाग में प्रारंभिक दिन गुजारे ? पार्क रोड के सामनेवाले घर में रहे। वहीं पहली बार मेरे साथ नवजात बेटी रही।
उसका घर का नाम भी वहीं काबुलीवाला फिल्म देखकर ‘मिनी’ रखा। वहाँ की साहित्यिक गोष्ठियों और वहाँ रहते हुए सूचना विभाग के सरकारी नौकरी के बीच अखंडित और अक्षत पाने का परितोष लेकर विश्वविद्यालय की चाकरी में प्रवेश हुआ। या फिर गोरखपुर में वहाँ के एक संयुक्त परिवार के साथ रहते हुए और अध्यापन में विभागीय प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते हुए अत्यंत सक्रिय और उतार-चढ़ाव भरे जीवन में इतना कुछ तीता हो सकता है, वह सब मैंने चखा और चखकर भी विशेष अनुग्रह इष्ट देवता का रहा होगा कि कुछ भी तीता नहीं हुआ। उसी अवधि में मैंने विदेश यात्राएँ शुरू कीं और लगभग तीन किस्तों में दीर्घ प्रवास के लेख बने। दीर्घ प्रवास के घरों को भी अपना घर कैसे न कहूँ, बल्कि उन्होंने अपने घर का आकर्षण प्रीतिकर बनाया। एक अन्य भिन्न संस्कृति के संघात ने अपने को अति दीप्त बनाया। केवल अपनी याद दिलाकर नहीं, बल्कि अपने स्वरूप की संपूर्ण पहचान एकदम भिन्न रंगवाली पिछवाई के रूप में बड़े स्पष्ट रूप से करवाई। या फिर बनारस को मैं घर कैसे न कहूँ जहाँ मैं सबसे अधिक अवधि तक रहा और कभी भी उस समय देश के बाहर नहीं गया। शुद्ध शास्त्रीय पंडितों के बीच में रहते हुए और संस्कृत का आदमी होकर आधुनिक भाषा और भाषा-विज्ञान विभाग का अध्यक्ष रहा। न सेतु रहा, न संत। दो नावों पर एक साथ सवार रहा, बल्कि मैं यों कहूँ, दो घोड़ों का संचालन करता था। कभी एक पर सवार रहता, कभी दूसरे पर; लेकिन दोनों को चलाता रहा। यह मेरी नियति रही-एक ओर लेखक रहा, दूसरी ओर अध्यापक, प्रशासक, और भी न जाने क्या-क्या रहा। लेखकवाला थोड़ा बड़ा, तो भी उसपर बैठने से ही इतनी क्षमता आई कि दूसरे घोड़े को भी सँभाल सका। इसके बाद ब्रजमंडल स्थित आगरे में करीब नौ वर्ष रहा। मन से वहाँ आगरे से अधिक वृंदावन में रहा। तन और मन के घरों को भी अपना घर कैसे न कहूँ ! सब जगहों में रहते हुए जो मेरा घर, एक विशिष्ट घर और वह भी चक्रमणशील का घर, बन गया था। उसको भी मैं घर कैसे न कहूँ, जहाँ सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहे। आज भी वे शब्द कानों को सुनाई देते हैं-‘आप बड़े गड़बड़ आदमी हैं। आपने कल आने को कहा था, कल क्यों नहीं आए ?
आपके आने को होता है तो न जाने कितने फोन पहले ही आ जाते हैं।
उस अपनी अनुपस्थिति के संकुल से भरनेवाला आदमी उस घर में इतना महत्त्व पाता था कि मेरा सामान तक सँभालकर रखते थे। भाई स्वयं पैक करते थे और एक-एक चीज इस ढंग से मेरे कमरे में रखी जाती थी। यह मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। आगरे से फिर लौटा तो बनारस। एक छोटे से घर में आया। दो-दो विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में। विपत्ति-जाल बँगलों में रहा और उन्हें भी घर कहना पड़ेगा। मेरा चलता तो मैं उन्हें जंगल कहता; लेकिन उन्हें जंगल नहीं कहूँगा। उससे बड़ा जंगल चेतना, संवेदना से शून्य अजनबियों का जंगल था। तीनेक साल मैं में दिल्ली रहा। कहने के लिए ऐश्य, पर वस्तुत: खालीपन के एक प्रयोग के बाद दूसरे प्रयोग करते हुए उसी के पूरा होने की कोशिश करता रहा। पर था तो वह भी बसेरा ही। केवल रात का नहीं, दिन-रात का बसेरा। सेहत के लिए लोग साइकिल चलाते रहते हैं और साइकिल एक इंच आगे नहीं बढ़ती है। वैसे ही पत्रकारिता का जीवन है, आप उड़ान भरते रहिए, पर एक इंच आगे नहीं जाते हैं। उस कर्ज से जल्दी छुट्टी ली। जल्दी मैं किसी से खीझता नहीं। खीझी हुई उक्ति है कि उस विराट् मरुस्थल में रहते हुए कई बार अमेरिका जाने का मौका लगा और वहाँ कई घर बन गए। ऐसे घर, जहाँ से लौटना कठिन हो जाता है। लोगों ने, दूर-दराज के भारतीय इतने स्वजन हो जाते हैं कि वे घर का और ‘घर’ शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। शायद बसेरा नहीं, घर है। पर है-अपरिचय का परिचय बनना। केवल बालपन की ही प्रीत नहीं छूटती, दूसरे जन्म के भी कुछ अहेतुकी संबंध होते हैं और एकाएक प्रकट होते हैं जो एक बार जुड़ जाते हैं तो नहीं छूटते हैं।
उसके बाद मैं बनारस में हूँ और अब शायद पाँच वर्ष हो रहे हैं। विदेश यात्राएँ अब भी हो रही हैं; पर बनारस में रहते हुए लगता है, यह तो घर भाव का ही महाश्मशान है। यह तो बेघरपन का घर है। इस घरपन में रहते हुए बसेरों की बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे किसी दूसरे बसेरे की तलाश है ? बसेरे की तलाश है तो क्या कंकड़ चुनने का मन या तन रह गया है ? वैसे तो मैंने किसी बसेरे के लिए कंकड़ नहीं चुना, पर आगे जिस बसेरे की खोज है उसके कंकड़ जरूर चुनूँगा। कंकड नहीं बल्कि तिनके, तरह-तरह के तिनके। हर तिनके का एक इतिहास है, जिसे तोड़ते हुए कोई बेमतलब की पर अंतरंग बात हुई है; जिसे भवभूति ने बेसिलसिले की बकवास कहा है, जिसमें रात ही बीत गई है और बातों का सिलसिला नहीं चुका है। इन तिनकों को चुनना इसलिए नहीं कि मैं घर को, इस रैन बसेरे को याद रखना चाहता हूँ, इसलिए कि इन तिनकों के साथ जुड़े रागात्मक संबंधों को किसी महाराग में रूपांतरित करना चाहता हूँ। असंख्य युवा-मनों और किशोर-मनों के भीतर उफनते हुए और उफनकर भी भीतर-ही-भीतर सिमटते हुए लजीले सपनों का रूपांतरण जैसा होता है, मदन-महोत्सव, वंसतोत्सव-वैसा ही कुछ रचना चाहता हूँ। एकदम कबीर, पलटूदास जैसे लोगों का निर्गुनिया उत्सव नहीं। ‘मोहन खेले फाग’ या ‘शिवशंकर खेले फाग’ वाला उत्सव।
शिवशंकर तो गौरा को संग लिये हुए फाग खेलते हैं, मोहन बेचारे के साथ तो यह है कि ‘वन-वन फूले टेसुआ, बगियन बेलि, चले बिदेस पियरवा, फगवा खेलि।’ दोनों फाग संग, सहयोग और विरह के फाग हैं- अपने-अपने ढंग के-समस्त लोक और विस्तार से कहें तो समस्त ब्रह्मांड के। इसमें सभी आश्रय हैं और सभी आलंबन। और सबसे मजे की बात यह है कि यह उत्सव असंख्य तिनकों को, तिनकोंवाले बसेरों को होलिका की आग में झोंककर उसी की राख से खेला जाता है। यह आग भी विचित्र है, तिनकों को राख बना देती है, बड़े-बड़े शहतीरों को भी राख बना देती है। पर संबंध राख में भी अपने सुवास छोड़ जाते हैं। उन्हीं संबंधों के इस रूपांतर से भक्ति का बीज पड़ता है, परानुरक्ति का बीज पड़ता है, सर्वस्य समर्पण का बीज पड़ता है। इसीलिए बसेरा मैंने स्वयं कभी बनाने की जहमत नहीं उठाई। जैसा जहाँ मिला उसे अपना लिया, उसके सुख-दु:ख अपना लिये, उसकी राग-रंगता अपनी ली। जब वहाँ से चला तब कुछ लिया नहीं, थोड़े से संबोधन छोड़ दिए। संबोधन के रूप में मैं बना रहा। लोगों को बसेरा बनाने में तल्लीन देखा तो लगा कि मुझे भी कोई बसेरा बनाना चाहिए; लेकिन ईंट-सीमेंटवाले आदमियों को देखते हुए मेरा संकल्प अपने आप बुझता रहा। और मैं देखता रहा स्वयं को एक अनजान देहरी से एक अत्यंत अपरिचय के आँगन में प्रवेश करते हुए। जीवन की देहरी-देहरी पर, जाने-पहचाने आँगन में प्रवेश करते हुए संतोष होता है-इस प्रपंच में मैं नहीं पड़ा। अपने ही शहर में देखता हूँ, पं.हजारीप्रसाद द्विवेदी ने घर बनाया, डॉ.राजबली पांडेय ने घर बनाया, पं.बलदेव उपाध्याय ने घर बनाया-और भी बहुत सारे विद्वानों ने, गुणवंतों ने घर बनाया और वे प्राय: सभी-के-सभी सूने हैं और उनमें रहनेवाले कोई है तो भी उन्हें कोई जानता नहीं है। इतना शानदार मकान चौधरी बदरीनायारण प्रेमघन का बिक गया। यह नहीं कि उनके उत्तराधिकारी असंपन्न थे। घर बनाने का अर्थ होता है घर रखाना, क्योंकि घर में जो आगे रहनेवाले हैं वे अपनी रुचि के घर में रहेंगे। इस पुरानी पड़ती डिजाइनवाले मकान में क्यों रहेंगे !
कम-से-कम मन से क्रम ठीक नहीं बन पाएगा। तब भी इन सभी घरों का, घरों की कोई-न-कोई गंध, कोई सुवास, कोई-न-कोई स्पर्श अभी तक प्राणों में हो, रोम-रोम में हो। इनमें से कोई भी ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं पराया कह सकूँ। कोई भी इनमें से मेरा नहीं है। पर मेरा जितना अपना होता है उससे अधिक अपना है। शायद इसीलिए इन सबके साथ बड़ा खट्टा-मीठा अनुभव जुड़ा हुआ है। भोजपुरी में इसे ‘अमलोन’ कहते हैं। और वैसा स्वाद अभी भी रसना में है, ललक बनी हुई है। अपभ्रंश में इसी को ‘अंबण’ कहते हैं और प्रिय के संदर्भ में किसी दोहे में यह कहा गया है कि प्रिय ने अमलोन स्वाद लगा दिया है। उसके लिए मोह अब भी है, मुँह में पानी भर आता है। कुछ ऐसा ही संबंध है कुछ ऐसी ही लाग...बसेरों में से प्रत्येक बसेरे ने लगा रखी है। मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता हूँ और दार्शनिक भाव से सोचना चाहता हूँ, ‘घर वही है जो थके को रैन भर का हो बसेरा।’ दार्शनिक भाव से वक्तव्य देना तो आसान है। ममता का आदमी के लिए खोखला होना कठिन है। ममता के त्याग की बात करते हैं। ममता का त्याग करेंगे तो आदमी कहाँ रहेगा। ममताओं का जाल जितना ही फैलता जाता है उतना ही आदमी का विस्तार होता है। ममता जितना बाँधती है उतना ही उसे कहीं मुक्त भी करती है। जितना अधिक जाल है, उस जाल को बढ़ाकर, तानकर तोड़ देने की कोशिश भी है, वह दायरा मात्र नहीं है। दायरों का ऐसा विस्तार है जिसमें दायरों की सीमा दिखती ही नहीं। जितनी वह कमजोरी है उससे अधिक आदमी की शक्ति है।
मैं यह सब विमर्श करते हुए दार्शनिक मुद्रा में फिर लौटना नहीं चाहता। मैं तो बस बसेरों की बात करना चाहता हूँ। बसेरों से अधिक, बसेरों को एक बार फिर, हर बार एक बसेरे में लौटकर, अपने को स्थापित करना चाहता हूँ। कर सकूँगा या नहीं, नहीं जानता। कोशिश करना चाहता हूँ। घर में रहनेवाला घर के बारे में नहीं सोचता। जितना घर से कई बार बाहर जाकर घर के बारे में सोचता है।
कोई पूछे, तुम्हारा घर कहाँ है ? तो मैं उत्तर देते समय लड़खड़ाने लगूँगा, किसे घर कहूँ ! जहाँ जन्म हुआ उसे, जो मेरे जन्म के दो-ढाई साल बाद ढहा दिया गया ? उसके बाद नया घर उठाया गया, उसे मानूँ ? छुट्टियों में ननिहाल के खंडहरनुमा घर में भारतेंदु काल के विपुल साहित्य के भंडार का आलोडन-विलोडन किया। अधिकतर समझ में नहीं आया। तरह-तरह के नाम आँखों के सामने तैरते हैं, उसे घर कहूँ, क्योंकि उस समय हिंदी में कुछ वैसा ही लिखने का मन जगा ? संस्कृत में जन्म हुआ। उसी ने मुझे पाला-पोसा और मैं उसी घर के कारण हिंदी के घर में चुपके से बैठने का संकल्प ले बैठा। या उसे घर कहूँ, जहाँ मैं रहा ? शहरवाले घर को घर कहूँ, जहाँ से मैंने स्कूली और प्रारंभिक शिक्षा पाई ? वहाँ चार घर बदले या घर इलाहाबाद के एक कोने से दूसरे कोने तक की अलग-अलग कोठरियों को घर कहूँ, जहाँ मैं ग्यारह वर्षों का समय कुछ अध्ययन और स्वावलंबनजीवी के संघर्ष में भिड़ा रहा ? या फिर विंध्य के दिन में तपते शाम, सियराते पहाड़ों-पत्थरों को फोड़कर बननेवाली नदियों, सिर से टकरानेवाली अटारियों और दरबारियों और भाषा के अतिशय विनम्रतावाली भाषा के बोलनेवाले, मित्रों के बीच पहले अजनबी की तरह सेवा छोड़ते-छोड़ते अपना पग दूसरे पड़ाव की ओर चला या फिर लखनऊ शहर के पं.भैया साहब श्रीनारायण चतुर्वेदी के उस मकान को जहाँ लखनऊ के सूचना विभाग में प्रारंभिक दिन गुजारे ? पार्क रोड के सामनेवाले घर में रहे। वहीं पहली बार मेरे साथ नवजात बेटी रही।
उसका घर का नाम भी वहीं काबुलीवाला फिल्म देखकर ‘मिनी’ रखा। वहाँ की साहित्यिक गोष्ठियों और वहाँ रहते हुए सूचना विभाग के सरकारी नौकरी के बीच अखंडित और अक्षत पाने का परितोष लेकर विश्वविद्यालय की चाकरी में प्रवेश हुआ। या फिर गोरखपुर में वहाँ के एक संयुक्त परिवार के साथ रहते हुए और अध्यापन में विभागीय प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते हुए अत्यंत सक्रिय और उतार-चढ़ाव भरे जीवन में इतना कुछ तीता हो सकता है, वह सब मैंने चखा और चखकर भी विशेष अनुग्रह इष्ट देवता का रहा होगा कि कुछ भी तीता नहीं हुआ। उसी अवधि में मैंने विदेश यात्राएँ शुरू कीं और लगभग तीन किस्तों में दीर्घ प्रवास के लेख बने। दीर्घ प्रवास के घरों को भी अपना घर कैसे न कहूँ, बल्कि उन्होंने अपने घर का आकर्षण प्रीतिकर बनाया। एक अन्य भिन्न संस्कृति के संघात ने अपने को अति दीप्त बनाया। केवल अपनी याद दिलाकर नहीं, बल्कि अपने स्वरूप की संपूर्ण पहचान एकदम भिन्न रंगवाली पिछवाई के रूप में बड़े स्पष्ट रूप से करवाई। या फिर बनारस को मैं घर कैसे न कहूँ जहाँ मैं सबसे अधिक अवधि तक रहा और कभी भी उस समय देश के बाहर नहीं गया। शुद्ध शास्त्रीय पंडितों के बीच में रहते हुए और संस्कृत का आदमी होकर आधुनिक भाषा और भाषा-विज्ञान विभाग का अध्यक्ष रहा। न सेतु रहा, न संत। दो नावों पर एक साथ सवार रहा, बल्कि मैं यों कहूँ, दो घोड़ों का संचालन करता था। कभी एक पर सवार रहता, कभी दूसरे पर; लेकिन दोनों को चलाता रहा। यह मेरी नियति रही-एक ओर लेखक रहा, दूसरी ओर अध्यापक, प्रशासक, और भी न जाने क्या-क्या रहा। लेखकवाला थोड़ा बड़ा, तो भी उसपर बैठने से ही इतनी क्षमता आई कि दूसरे घोड़े को भी सँभाल सका। इसके बाद ब्रजमंडल स्थित आगरे में करीब नौ वर्ष रहा। मन से वहाँ आगरे से अधिक वृंदावन में रहा। तन और मन के घरों को भी अपना घर कैसे न कहूँ ! सब जगहों में रहते हुए जो मेरा घर, एक विशिष्ट घर और वह भी चक्रमणशील का घर, बन गया था। उसको भी मैं घर कैसे न कहूँ, जहाँ सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहे। आज भी वे शब्द कानों को सुनाई देते हैं-‘आप बड़े गड़बड़ आदमी हैं। आपने कल आने को कहा था, कल क्यों नहीं आए ?
आपके आने को होता है तो न जाने कितने फोन पहले ही आ जाते हैं।
उस अपनी अनुपस्थिति के संकुल से भरनेवाला आदमी उस घर में इतना महत्त्व पाता था कि मेरा सामान तक सँभालकर रखते थे। भाई स्वयं पैक करते थे और एक-एक चीज इस ढंग से मेरे कमरे में रखी जाती थी। यह मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। आगरे से फिर लौटा तो बनारस। एक छोटे से घर में आया। दो-दो विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में। विपत्ति-जाल बँगलों में रहा और उन्हें भी घर कहना पड़ेगा। मेरा चलता तो मैं उन्हें जंगल कहता; लेकिन उन्हें जंगल नहीं कहूँगा। उससे बड़ा जंगल चेतना, संवेदना से शून्य अजनबियों का जंगल था। तीनेक साल मैं में दिल्ली रहा। कहने के लिए ऐश्य, पर वस्तुत: खालीपन के एक प्रयोग के बाद दूसरे प्रयोग करते हुए उसी के पूरा होने की कोशिश करता रहा। पर था तो वह भी बसेरा ही। केवल रात का नहीं, दिन-रात का बसेरा। सेहत के लिए लोग साइकिल चलाते रहते हैं और साइकिल एक इंच आगे नहीं बढ़ती है। वैसे ही पत्रकारिता का जीवन है, आप उड़ान भरते रहिए, पर एक इंच आगे नहीं जाते हैं। उस कर्ज से जल्दी छुट्टी ली। जल्दी मैं किसी से खीझता नहीं। खीझी हुई उक्ति है कि उस विराट् मरुस्थल में रहते हुए कई बार अमेरिका जाने का मौका लगा और वहाँ कई घर बन गए। ऐसे घर, जहाँ से लौटना कठिन हो जाता है। लोगों ने, दूर-दराज के भारतीय इतने स्वजन हो जाते हैं कि वे घर का और ‘घर’ शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। शायद बसेरा नहीं, घर है। पर है-अपरिचय का परिचय बनना। केवल बालपन की ही प्रीत नहीं छूटती, दूसरे जन्म के भी कुछ अहेतुकी संबंध होते हैं और एकाएक प्रकट होते हैं जो एक बार जुड़ जाते हैं तो नहीं छूटते हैं।
उसके बाद मैं बनारस में हूँ और अब शायद पाँच वर्ष हो रहे हैं। विदेश यात्राएँ अब भी हो रही हैं; पर बनारस में रहते हुए लगता है, यह तो घर भाव का ही महाश्मशान है। यह तो बेघरपन का घर है। इस घरपन में रहते हुए बसेरों की बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे किसी दूसरे बसेरे की तलाश है ? बसेरे की तलाश है तो क्या कंकड़ चुनने का मन या तन रह गया है ? वैसे तो मैंने किसी बसेरे के लिए कंकड़ नहीं चुना, पर आगे जिस बसेरे की खोज है उसके कंकड़ जरूर चुनूँगा। कंकड नहीं बल्कि तिनके, तरह-तरह के तिनके। हर तिनके का एक इतिहास है, जिसे तोड़ते हुए कोई बेमतलब की पर अंतरंग बात हुई है; जिसे भवभूति ने बेसिलसिले की बकवास कहा है, जिसमें रात ही बीत गई है और बातों का सिलसिला नहीं चुका है। इन तिनकों को चुनना इसलिए नहीं कि मैं घर को, इस रैन बसेरे को याद रखना चाहता हूँ, इसलिए कि इन तिनकों के साथ जुड़े रागात्मक संबंधों को किसी महाराग में रूपांतरित करना चाहता हूँ। असंख्य युवा-मनों और किशोर-मनों के भीतर उफनते हुए और उफनकर भी भीतर-ही-भीतर सिमटते हुए लजीले सपनों का रूपांतरण जैसा होता है, मदन-महोत्सव, वंसतोत्सव-वैसा ही कुछ रचना चाहता हूँ। एकदम कबीर, पलटूदास जैसे लोगों का निर्गुनिया उत्सव नहीं। ‘मोहन खेले फाग’ या ‘शिवशंकर खेले फाग’ वाला उत्सव।
शिवशंकर तो गौरा को संग लिये हुए फाग खेलते हैं, मोहन बेचारे के साथ तो यह है कि ‘वन-वन फूले टेसुआ, बगियन बेलि, चले बिदेस पियरवा, फगवा खेलि।’ दोनों फाग संग, सहयोग और विरह के फाग हैं- अपने-अपने ढंग के-समस्त लोक और विस्तार से कहें तो समस्त ब्रह्मांड के। इसमें सभी आश्रय हैं और सभी आलंबन। और सबसे मजे की बात यह है कि यह उत्सव असंख्य तिनकों को, तिनकोंवाले बसेरों को होलिका की आग में झोंककर उसी की राख से खेला जाता है। यह आग भी विचित्र है, तिनकों को राख बना देती है, बड़े-बड़े शहतीरों को भी राख बना देती है। पर संबंध राख में भी अपने सुवास छोड़ जाते हैं। उन्हीं संबंधों के इस रूपांतर से भक्ति का बीज पड़ता है, परानुरक्ति का बीज पड़ता है, सर्वस्य समर्पण का बीज पड़ता है। इसीलिए बसेरा मैंने स्वयं कभी बनाने की जहमत नहीं उठाई। जैसा जहाँ मिला उसे अपना लिया, उसके सुख-दु:ख अपना लिये, उसकी राग-रंगता अपनी ली। जब वहाँ से चला तब कुछ लिया नहीं, थोड़े से संबोधन छोड़ दिए। संबोधन के रूप में मैं बना रहा। लोगों को बसेरा बनाने में तल्लीन देखा तो लगा कि मुझे भी कोई बसेरा बनाना चाहिए; लेकिन ईंट-सीमेंटवाले आदमियों को देखते हुए मेरा संकल्प अपने आप बुझता रहा। और मैं देखता रहा स्वयं को एक अनजान देहरी से एक अत्यंत अपरिचय के आँगन में प्रवेश करते हुए। जीवन की देहरी-देहरी पर, जाने-पहचाने आँगन में प्रवेश करते हुए संतोष होता है-इस प्रपंच में मैं नहीं पड़ा। अपने ही शहर में देखता हूँ, पं.हजारीप्रसाद द्विवेदी ने घर बनाया, डॉ.राजबली पांडेय ने घर बनाया, पं.बलदेव उपाध्याय ने घर बनाया-और भी बहुत सारे विद्वानों ने, गुणवंतों ने घर बनाया और वे प्राय: सभी-के-सभी सूने हैं और उनमें रहनेवाले कोई है तो भी उन्हें कोई जानता नहीं है। इतना शानदार मकान चौधरी बदरीनायारण प्रेमघन का बिक गया। यह नहीं कि उनके उत्तराधिकारी असंपन्न थे। घर बनाने का अर्थ होता है घर रखाना, क्योंकि घर में जो आगे रहनेवाले हैं वे अपनी रुचि के घर में रहेंगे। इस पुरानी पड़ती डिजाइनवाले मकान में क्यों रहेंगे !
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book